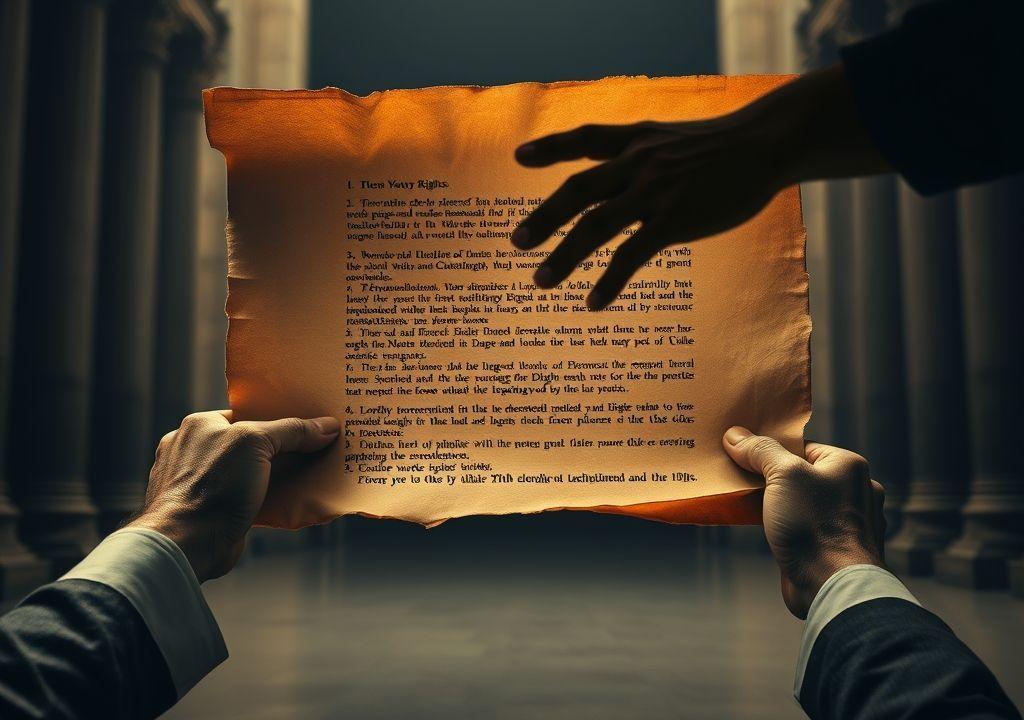बिहार से संसद तक: वोटर वेरिफिकेशन पर काले कपड़े और सदन की मर्यादा का प्रश्न
चर्चा में क्यों? (Why in News?):
भारतीय लोकतंत्र का हृदय, हमारी संसद, एक बार फिर गहन विचार-विमर्श से अधिक तीखे विरोध प्रदर्शनों का गवाह बनी। हाल ही में, बिहार में चल रहे मतदाता सत्यापन (Voter Verification) अभियान को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इतना तीव्र था कि सांसदों ने सदन के ‘वेल’ तक पहुँचकर नारेबाजी की, जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष ओम बिरला को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी कि “सड़क का व्यवहार सदन में न करें”। यह घटना न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है, बल्कि संसदीय मर्यादा और विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन को भी रेखांकित करती है। यह लेख इस घटना की गहराई में जाकर, इसके विभिन्न आयामों, चुनावी प्रक्रिया के महत्व, संसदीय परंपराओं और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण करेगा, जो UPSC उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका होगी।
मतदाता सत्यापन: लोकतंत्र की बुनियाद का सुरक्षा कवच
किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का आधार मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची जितनी सटीक और अद्यतन होगी, चुनाव परिणाम उतने ही विश्वसनीय होंगे। यहीं पर मतदाता सत्यापन की भूमिका आती है।
क्या है मतदाता सत्यापन?
मतदाता सत्यापन (Voter Verification) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों की सत्यता, निवास स्थान और पात्रता की जाँच की जाती है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं को शामिल करना है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक और योग्य नागरिक ही मतदान कर सकें।
क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण?
- निष्पक्ष चुनाव की गारंटी: सटीक मतदाता सूची धांधली, फर्जी मतदान और चुनावी धोखाधड़ी की संभावना को कम करती है।
- प्रतिनिधित्व की शुद्धता: यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में जनसंख्या के सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लोकतंत्र में विश्वास: एक विश्वसनीय मतदाता सूची नागरिकों का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाती है, जिससे वे अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- संसाधनों का कुशल उपयोग: अद्यतन सूची अनावश्यक मतदान सामग्री और बूथ प्रबंधन लागत को कम करती है।
कानूनी आधार और प्रक्रिया
भारत में मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के प्रावधानों का पालन किया जाता है।
मुख्य प्रक्रियाएँ:
- निरंतर अद्यतन (Continuous Updation): नए मतदाताओं को पंजीकृत करना और मृत/स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना एक सतत प्रक्रिया है।
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR): प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि में, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के एक विशेष पुनरीक्षण अभियान की घोषणा करता है, जहाँ दावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया जाता है।
- घर-घर सत्यापन: कई बार, निर्वाचन अधिकारी (EROs) या उनके प्रतिनिधि घर-घर जाकर जानकारी सत्यापित करते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल और शिविर: नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल या विशेष शिविरों के माध्यम से अपने विवरण को सत्यापित करने, सुधारने या नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाता है।
बिहार में हालिया घटना के केंद्र में इसी सत्यापन प्रक्रिया के क्रियान्वयन को लेकर चिंताएँ थीं।
बिहार के संदर्भ में विशिष्ट चिंताएँ: क्यों उठा विरोध का बवंडर?
विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन बिहार में चल रहे मतदाता सत्यापन अभियान में कथित विसंगतियों और पारदर्शिता की कमी से उपजा था। उनके आरोप निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित थे:
- मनमाने ढंग से नाम हटाना: विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं, खासकर कुछ विशिष्ट समुदायों और क्षेत्रों से। यह आरोप लगाया गया कि यह प्रक्रिया बिना उचित सत्यापन या नोटिस के की जा रही है।
- प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी: सांसदों ने दावा किया कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। मतदाताओं को पर्याप्त नोटिस नहीं दिए जा रहे हैं, और उनके पास अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने का पर्याप्त अवसर नहीं है।
- राजनीतिक प्रेरणा: विपक्ष ने आशंका व्यक्त की कि इस सत्यापन अभियान का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है ताकि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चुनावी परिदृश्य को बदला जा सके।
- मतदान के अधिकार का हनन: यदि योग्य मतदाताओं के नाम बिना कारण हटा दिए जाते हैं, तो यह उनके संवैधानिक मतदान के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
“लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि हर नागरिक की आवाज़ का सम्मान है। यदि सत्यापन के नाम पर किसी की आवाज़ दबाई जाती है, तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।”
इन चिंताओं ने विपक्षी सांसदों को संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर एक संभावित हमला था।
संसदीय मर्यादा बनाम विरोध का अधिकार: एक जटिल संतुलन
संसद सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है; यह वह मंच है जहाँ राष्ट्र की आवाज़ गूँजती है, जहाँ सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है, और जहाँ विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। हालांकि, इस अभिव्यक्ति के लिए कुछ नियम और मर्यादाएँ निर्धारित की गई हैं, ताकि सदन की गरिमा और कार्यप्रणाली बनी रहे।
संसद का उद्देश्य और नियम
हमारी संसद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के लिए कानून बनाना, बजट पर चर्चा करना, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बहस करना और सरकार पर नियंत्रण रखना है। इन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपने ‘कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम’ (Rules of Procedure and Conduct of Business) होते हैं। ये नियम सांसदों के आचरण, बहस के तरीके और सदन की गरिमा बनाए रखने से संबंधित होते हैं।
- सदन का ‘वेल’ (Well of the House): यह अध्यक्ष की सीट के ठीक सामने का वह खुला क्षेत्र होता है जहाँ सदन के कर्मचारी बैठते हैं। नियमों के अनुसार, सांसदों को अध्यक्ष की अनुमति के बिना ‘वेल’ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। वेल में प्रवेश करना अक्सर विरोध का एक तीव्र रूप माना जाता है जो सदन की कार्यवाही को बाधित करता है।
- अध्यक्ष की भूमिका: अध्यक्ष (लोकसभा स्पीकर) सदन के संरक्षक होते हैं। वे कार्यवाही का संचालन करते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं, और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। अध्यक्ष के पास अशांति फैलाने वाले सदस्यों को निलंबित करने या सदन की कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति होती है।
विरोध प्रदर्शन का अधिकार और इसकी सीमाएँ
लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना, जनहित के मुद्दों को उठाना और सरकार को उसकी जवाबदेही के प्रति सचेत करना है। इसके लिए, सांसदों को सदन के भीतर अपनी बात रखने, सवाल पूछने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।
विरोध के सामान्य तरीके:
- प्रश्नकाल और शून्यकाल में प्रश्न उठाना।
- स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
- बहस में भाग लेना और असहमति व्यक्त करना।
- वॉकआउट (सदन से बाहर जाना)।
- नारेबाजी (कुछ सीमाओं के भीतर)।
हालांकि, जब विरोध प्रदर्शन सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करता है, या जब सांसद ‘वेल’ में आते हैं, तो इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। अध्यक्ष का यह बयान कि “सड़क का व्यवहार सदन में न करें” इसी संदर्भ में आया था। यह इस बात पर जोर देता है कि संसद में विरोध का एक तरीका होता है जो उसकी गरिमा के अनुरूप हो, न कि ऐसा जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या सम्मान भंग हो।
“विरोध लोकतंत्र का प्राणवायु है, पर सदन उसकी फेफड़े हैं। यदि फेफड़े ही ठीक से काम न करें, तो प्राणवायु भी निरर्थक हो जाती है।”
यहां चुनौती यह है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले, वहीं सदन को अपना विधायी कार्य भी सुचारू रूप से करना चाहिए। बार-बार होने वाले व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण विधेयकों और चर्चाओं में बाधा डालते हैं, बल्कि जनता के मन में संसद की छवि को भी धूमिल करते हैं।
लोकतंत्र पर निहितार्थ: गहराता संकट या सशक्त अभिव्यक्ति?
बिहार वोटर सत्यापन विवाद और संसद में हुए विरोध प्रदर्शन के भारतीय लोकतंत्र पर कई गहरे निहितार्थ हैं:
संस्थागत विश्वास का क्षरण
जब मतदाता सत्यापन जैसी मूलभूत प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और संसद में इस पर हंगामा होता है, तो इससे जनता का चुनाव आयोग और संसदीय संस्थानों पर विश्वास कम हो सकता है। यदि लोग चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं मानते हैं, तो वे मतदान में रुचि खो सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
संसदीय कार्यप्रणाली पर प्रभाव
लगातार व्यवधानों और विरोध प्रदर्शनों से संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती, नीति निर्माण प्रभावित होता है, और सरकार की जवाबदेही तय करने का अवसर खो जाता है। संसद बहस और विचार-विमर्श का केंद्र है, न कि केवल विरोध प्रदर्शन का अखाड़ा।
विपक्ष की भूमिका पर बहस
यह घटना विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाती है। क्या तीव्र विरोध ही एकमात्र प्रभावी तरीका है? क्या सदन में मुद्दों को उठाने के लिए रचनात्मक और नियम-आधारित तरीके उपलब्ध नहीं हैं? अक्सर, जब गतिरोध होता है, तो यह विपक्ष की प्रभावी विधायी भूमिका को कमजोर करता है, भले ही उनका इरादा नेक हो।
सार्वजनिक धारणा
जनता, जो टीवी पर संसदीय कार्यवाही देखती है, अक्सर सांसदों को हंगामा करते और नारे लगाते हुए पाती है। इससे राजनीति और राजनेताओं के प्रति नकारात्मक धारणा बनती है। वे सांसदों को गंभीर मुद्दों पर बहस करने के बजाय केवल शोर मचाते हुए देखते हैं, जिससे लोकतंत्र की छवि धूमिल होती है।
प्रशासकीय सुधारों की आवश्यकता
मतदाता सत्यापन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उठाए गए सवालों से यह भी पता चलता है कि चुनाव आयोग और संबंधित प्रशासनिक निकायों को अपनी प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता है। यदि प्रक्रिया में खामियाँ हैं या उसकी धारणा ही खराब है, तो वह अविश्वास को जन्म देती है।
आगे की राह: सशक्त लोकतंत्र की ओर
इस घटना से उबरने और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता है:
1. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही
- स्पष्ट दिशानिर्देश और संचार: निर्वाचन आयोग को मतदाता सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। आम जनता और राजनीतिक दलों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र: मतदाताओं के लिए अपने नामों के गलत तरीके से हटाए जाने या अपात्रता के मामलों में त्वरित और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। अपील की प्रक्रिया सरल और सुलभ होनी चाहिए।
- बहु-हितधारक परामर्श: सत्यापन अभियान शुरू करने से पहले, निर्वाचन आयोग को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और प्रक्रिया में विश्वास पैदा किया जा सके।
- तकनीकी उन्नयन: डेटा प्रबंधन और सत्यापन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मानव हस्तक्षेप और सत्यापन की आवश्यकता बनी रहेगी।
2. संसदीय मर्यादा और संवाद को प्रोत्साहन
- नियमों का पालन: सांसदों को सदन के नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- संवाद और सर्वसम्मति: सरकार और विपक्ष दोनों को प्रमुख मुद्दों पर रचनात्मक संवाद में शामिल होना चाहिए। गतिरोध को तोड़ने के लिए अनौपचारिक बैठकें और सर्वदलीय बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- अध्यक्ष की भूमिका: अध्यक्ष को न केवल नियमों को लागू करना चाहिए, बल्कि सभी दलों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष अवसर भी प्रदान करना चाहिए, ताकि विपक्ष को वेल में आने की आवश्यकता महसूस न हो।
- संसदीय समितियों का सदुपयोग: महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों को अधिक गहन विचार-विमर्श के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा जाना चाहिए, जहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विशेषज्ञ राय पर विचार किया जा सके।
“संसद सिर्फ टकराव का अखाड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मंदिर है। यहाँ संवाद और सहयोग से ही वास्तविक प्रगति संभव है।”
3. राजनीतिक परिपक्वता और सार्वजनिक शिक्षा
- नैतिक आचरण: सभी राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों से उच्च नैतिक मानकों और संसदीय आचरण की अपेक्षा करनी चाहिए।
- जन जागरूकता: मीडिया और नागरिक समाज संगठनों को संसदीय प्रक्रियाओं, चुनावी सुधारों और लोकतंत्र के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने में भूमिका निभानी चाहिए।
निष्कर्ष
बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर संसद में हुए विरोध प्रदर्शन ने भारतीय लोकतंत्र की कुछ मूलभूत चुनौतियों को उजागर किया है: चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना, संसदीय मर्यादा का सम्मान करना, और विरोध के अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना। यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है जिसे निरंतर पोषण और सुधार की आवश्यकता होती है। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और स्वयं नागरिक सभी की इसमें भूमिका है। यदि हम अपने संस्थानों में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी, नियमों का सम्मान करना होगा और रचनात्मक संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना सीखना होगा। तभी हम एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे जो न केवल मजबूत हो, बल्कि हर नागरिक की आवाज़ का सच्चा प्रतिबिंब भी हो।
UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs
(यहां 10 MCQs, उनके उत्तर और व्याख्या प्रदान करें)
-
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत में मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा नियंत्रित होता है।
- मतदाता सूची से डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाना मतदाता सत्यापन का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक वार्षिक प्रक्रिया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (b)
व्याख्या: कथन (a) गलत है क्योंकि मतदाता सूची का कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 दोनों द्वारा नियंत्रित होता है। कथन (b) सही है क्योंकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं को हटाना महत्वपूर्ण है। कथन (c) सही है, SSR निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रक्रिया है।
-
भारतीय संसद के संदर्भ में, ‘वेल ऑफ द हाउस’ (Well of the House) शब्द का क्या अर्थ है?
(a) अध्यक्ष के आसन के पीछे का क्षेत्र जहाँ अधिकारी बैठते हैं।
(b) सदन के भीतर वह क्षेत्र जहाँ केवल मंत्री बैठ सकते हैं।
(c) अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक सामने का खुला क्षेत्र जहाँ सदन के कर्मचारी बैठते हैं।
(d) वह गैलरी जहाँ मीडिया के प्रतिनिधि बैठते हैं।
उत्तर: (c)
व्याख्या: ‘वेल ऑफ द हाउस’ अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक सामने का खुला क्षेत्र होता है, जहाँ सदन के कर्मचारी (जैसे रिपोर्टर, क्लर्क) बैठते हैं। सांसदों को अध्यक्ष की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, और वेल में आना अक्सर विरोध का एक तीव्र रूप माना जाता है।
-
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(a) यह संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में भ्रष्टाचार और चुनावी अपराधों से संबंधित है।
(b) यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन से संबंधित है।
(c) यह मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है।
(d) यह चुनाव याचिकाओं और उपचुनावों के आयोजन से संबंधित है।
उत्तर: (c)
व्याख्या: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मुख्य रूप से मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन से संबंधित है। जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन, चुनावी अपराधों और विवादों से संबंधित है।
-
भारत में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है, और यह भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (b)
व्याख्या: कथन (a) और (b) सही हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को व्यापक शक्तियां देता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। कथन (c) गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है, और यह भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य नहीं करता है; यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत किया गया है।
-
संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) संसद के सदस्य संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
(b) एक सांसद को सिविल मामलों में संसद सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
(c) आपराधिक मामलों में संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं होते हैं।
(d) अध्यक्ष को सदन में अव्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सदस्य को बिना किसी कारण के तुरंत निलंबित करने का अधिकार है।
उत्तर: (d)
व्याख्या: कथन (a), (b), (c) सभी सही हैं। सांसदों को सदन में अपने भाषण और कार्यवाहियों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्राप्त है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। कथन (d) गलत है। अध्यक्ष के पास सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन यह ‘बिना किसी कारण’ नहीं होता, बल्कि सदन के नियमों के उल्लंघन और अव्यवस्था फैलाने के कारण होता है, और इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं (जैसे नाम पुकारना, प्रस्ताव पारित करना)।
-
भारत में मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों में शामिल हो सकते हैं:
- डोर-टू-डोर सत्यापन।
- मतदाताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं सत्यापन।
- मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से व्यक्तिगत सत्यापन।
- मृत मतदाताओं के रिकॉर्ड का सरकारी डेटाबेस से मिलान।
सही संयोजन चुनें:
(a) 1, 2 और 3 केवल
(b) 2, 3 और 4 केवल
(c) 1, 2 और 4 केवल
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (d)
व्याख्या: निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन सभी तरीकों का उपयोग करता है। डोर-टू-डोर सत्यापन, ऑनलाइन सत्यापन, मतदाता सूचना पर्ची (हालांकि यह एक सत्यापन विधि से अधिक जानकारी देने की विधि है, पर इसमें भी मतदाता को अपना विवरण जांचने का मौका मिलता है), और विभिन्न सरकारी डेटाबेस से मिलान सभी महत्वपूर्ण तरीके हैं।
-
संसद में विरोध प्रदर्शन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
- संसद में ‘वॉकआउट’ (Walkout) करना विरोध प्रदर्शन का एक स्वीकृत तरीका है, लेकिन यह सदन के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
- नारेबाजी करना और तख्तियां दिखाना हमेशा संसदीय मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए तुरंत निलंबन किया जा सकता है।
- विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों का रचनात्मक समर्थन करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (a)
व्याख्या: कथन (a) सही है। वॉकआउट विरोध का एक सामान्य और स्वीकृत तरीका है। कथन (b) गलत है। नारेबाजी और तख्तियां दिखाना अक्सर मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा ‘तुरंत’ निलंबन का कारण नहीं बनता, और इसके लिए अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार तख्तियां दिखाना प्रतिबंधित है, लेकिन नारेबाजी की तीव्रता और संदर्भ मायने रखता है। कथन (c) गलत है। विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसे जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना है, न कि केवल समर्थन करना।
-
लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अंतिम संरक्षक होता है।
- वह किसी विधेयक के ‘धन विधेयक’ होने का अंतिम निर्णय लेता है, और यह निर्णय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- वह सदन में ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के तहत सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने वाला अंतिम प्राधिकारी है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (c)
व्याख्या: सभी तीनों कथन सही हैं। अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर उसका निर्णय अंतिम होता है और आमतौर पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (हालांकि किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा बताया था, लेकिन धन विधेयक के मामले में स्थिति अलग है)। इसके अलावा, दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।
-
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव से संबंधित प्रावधानों में शामिल हैं:
- चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण।
- सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मानदंड।
- उप-चुनाव और आकस्मिक रिक्तियों को भरना।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (c)
व्याख्या: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन, चुनावी अपराधों, भ्रष्ट आचरण, और सांसदों/विधायकों की अयोग्यता से संबंधित व्यापक प्रावधानों को कवर करता है। इसमें उपचुनावों और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के तरीके भी शामिल हैं।
-
भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (Delimitation) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
- परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर सीटों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
उत्तर: (b)
व्याख्या: कथन (a) गलत है। परिसीमन आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत किया जाता है। कथन (b) सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ताकि प्रक्रिया में देरी से बचा जा सके। कथन (c) सही है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
मुख्य परीक्षा (Mains)
(यहां 3-4 मेन्स के प्रश्न प्रदान करें)
- “संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का अधिकार, संसदीय मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित होना चाहिए।” हाल ही में बिहार में मतदाता सत्यापन पर संसद में हुए हंगामे के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (250 शब्द, 15 अंक)
- भारत में मतदाता सूची के शुद्धिकरण और सत्यापन की प्रक्रियाएँ निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, मौजूदा चुनौतियों का विश्लेषण करें और इस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव दें। (250 शब्द, 15 अंक)
- “सड़क का व्यवहार सदन में न करें।” लोकसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी संसदीय कार्यवाही में बढ़ते व्यवधानों पर एक गंभीर चिंता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर संसद में लगातार होने वाले गतिरोधों के प्रभावों का मूल्यांकन करें। इन गतिरोधों को कम करने और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
[कोर्स और फ्री नोट्स के लिए यहाँ क्लिक करें]