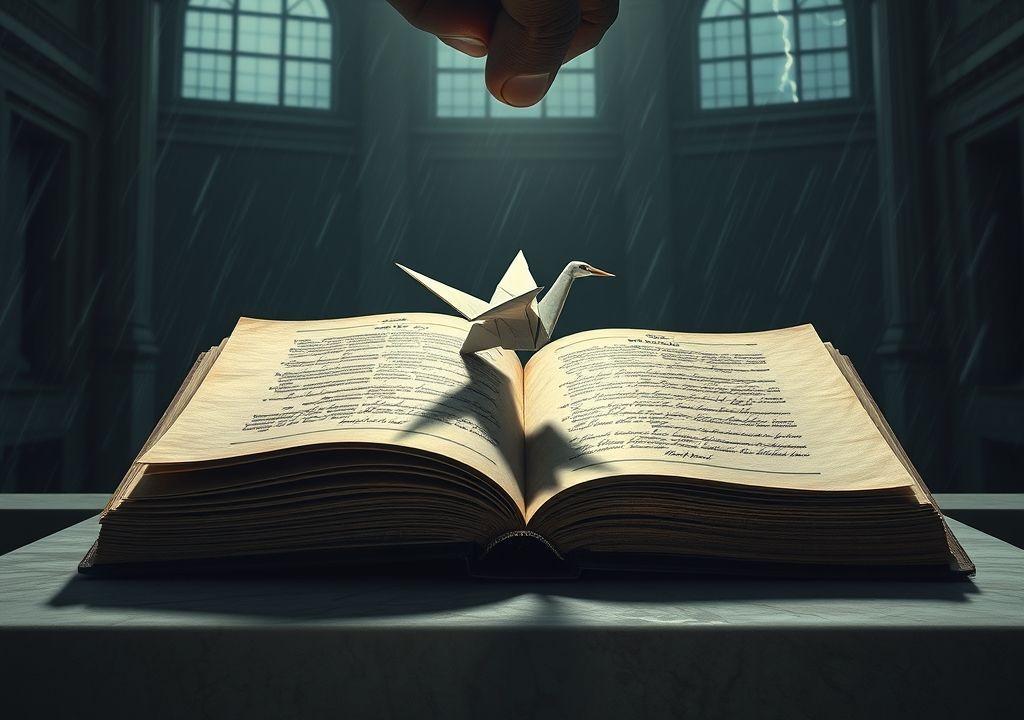पहलगाम-सीजफायर पर मोदी सरकार से जवाबदेही: संसद के मानसून सत्र की बड़ी चुनौती
चर्चा में क्यों? (Why in News?):
हाल ही में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार से ‘पहलगाम-सीजफायर’ मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है। विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वे मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है। यह घटनाक्रम आगामी संसदीय सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकार की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद के महत्व पर तीखी बहस का संकेत देता है, जो UPSC उम्मीदवारों के लिए संसदीय कार्यवाही, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और संघीय व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है।
पहलगाम ‘सीजफायर’ विवाद क्या है?
पहलगाम जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता के कारण यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कड़ी रहती है। जब विपक्ष ‘पहलगाम-सीजफायर’ पर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो यह कई संभावित आयामों की ओर इशारा करता है:
- सुरक्षा चूक का आरोप: विपक्ष का आरोप हो सकता है कि पहलगाम या उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर कोई समझौता किया गया है, या किसी विशेष सुरक्षा ऑपरेशन में ‘सीजफायर’ (संघर्ष विराम) जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अप्रिय घटना घटी हो या राष्ट्रीय हितों से समझौता हुआ हो। यह एक गुप्त सुरक्षा नीति या ऑपरेशनल निर्णय पर सवाल उठा सकता है।
- अशांत स्थिति की व्याख्या: यह संभव है कि विपक्ष किसी विशिष्ट घटना, आतंकवादी गतिविधि या सीमा पार से घुसपैठ को ‘सीजफायर’ के उल्लंघन के रूप में देख रहा हो, जिस पर सरकार ने संतोषजनक प्रतिक्रिया न दी हो या स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही हो। ‘सीजफायर’ शब्द का प्रयोग यहाँ एक व्यापक अर्थ में किया जा सकता है, जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई में किसी कथित ढिलाई या दुश्मन की ओर से हमले की स्थिति को संदर्भित करता हो, जिस पर सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
- खुफिया जानकारी पर आधारित चिंताएं: यह भी हो सकता है कि विपक्ष के पास कुछ विशिष्ट खुफिया जानकारी हो, जो पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित किसी संवेदनशील स्थिति या सरकार की गुप्त रणनीति की ओर इशारा करती हो, जिसे सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- राजनीतिक दबाव और पारदर्शिता: कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी कोई भी मुद्दा गंभीर राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है। यह सरकार की नीति निर्माण, संचालन क्षमता और खुफिया तंत्र पर सवाल उठा रहा है।
यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या सरकार ने पहलगाम क्षेत्र में किसी अनौपचारिक या औपचारिक ‘सीजफायर’ जैसी स्थिति को संभाला है, या क्या किसी सुरक्षा संबंधी घटना को ‘सीजफायर’ के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए और सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। विपक्ष का मानना है कि यह मुद्दा इतना गंभीर है कि सीधे प्रधानमंत्री को इस पर सदन में जवाब देना चाहिए।
विपक्ष की चिंताएं और सरकार की जवाबदेही: लोकतंत्र के स्तंभ
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह ठहराना और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं, तो यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
विपक्ष की भूमिका और चिंताएं:
- सरकार पर निगरानी: विपक्ष सरकार के कामकाज, नीतियों और निर्णयों पर निरंतर निगरानी रखता है। ‘पहलगाम-सीजफायर’ जैसे मुद्दे को उठाकर, विपक्ष सरकार से संवेदनशील सुरक्षा मामलों पर स्पष्टीकरण और पारदर्शिता की मांग कर रहा है।
- सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व: राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सीधे देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। विपक्ष जनता की उन आशंकाओं को आवाज देता है जो किसी संभावित सुरक्षा चूक या नीतिगत अस्पष्टता के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।
- नीतिगत बहस का सूत्रधार: विपक्ष सरकार की नीतियों की कमियों को उजागर कर उन्हें बेहतर बनाने के लिए दबाव डालता है। पहलगाम पर बहस से सरकार को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने या उसे स्पष्ट करने का अवसर मिल सकता है।
- शासन में संतुलन: एक मजबूत विपक्ष सरकार को निरंकुश होने से रोकता है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करता है। यह विधायिका को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।
सरकार की जवाबदेही:
लोकतांत्रिक प्रणाली में, कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है। इसका अर्थ है कि सरकार को अपने प्रत्येक निर्णय और कार्य के लिए संसद को स्पष्टीकरण देना होता है।
- पारदर्शिता और स्पष्टीकरण: सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर उठाई गई चिंताओं का जवाब दे। प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री द्वारा सदन में दिया गया जवाब जनता के बीच विश्वास बहाल करता है।
- सार्वजनिक विश्वास: जब सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है और जनता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देती है, तो इससे सार्वजनिक विश्वास मजबूत होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पर लोगों का भरोसा बना रहता है।
- संसदीय मर्यादा और परंपराएं: संसदीय लोकतंत्र में यह एक स्थापित परंपरा है कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद में चर्चा करती है और जवाब देती है। यह संसदीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक है।
- समस्या का समाधान: सवालों का जवाब देने से न केवल सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, बल्कि यह किसी भी संभावित समस्या का समाधान खोजने में भी मदद करता है। यदि वास्तव में कोई सुरक्षा चूक हुई है, तो उसे स्वीकार करके सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
“एक जीवंत लोकतंत्र में, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, और सरकार का काम ईमानदारी से जवाब देना है। यह प्रक्रिया ही जवाबदेही सुनिश्चित करती है।”
पहलगाम-सीजफायर मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन और जवाबदेही के सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं। आगामी मानसून सत्र में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठा पाता है।
संसद और संसदीय मर्यादाएं: वाद-विवाद का पवित्र मंदिर
संसद भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जो देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह ठहराने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करने का प्राथमिक मंच है।
संसद की भूमिका और महत्व:
- विधायन: संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है। यह मौजूदा कानूनों में संशोधन भी करती है।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद विभिन्न उपकरणों (जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव) के माध्यम से कार्यपालिका (सरकार) को जवाबदेह ठहराती है।
- वित्तीय नियंत्रण: संसद सरकारी खर्चों को अधिकृत करती है और कर प्रस्तावों को मंजूरी देती है, जिससे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- बहस और चर्चा का मंच: यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर व्यापक बहस और चर्चा का मंच प्रदान करता है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं।
- संविधान संशोधन: संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।
सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) का महत्व:
सर्वदलीय बैठकें संसद सत्र शुरू होने से पहले या महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए बुलाई जाती हैं। इनका उद्देश्य है:
- सहयोग को बढ़ावा देना: विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना।
- सत्र की योजना: आगामी सत्र के एजेंडा और कार्यप्रणाली पर चर्चा करना ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।
- मुद्दों को समझना: विपक्ष की चिंताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना ताकि सदन में व्यवधानों को कम किया जा सके।
- सरकार की पहल: सरकार अपनी विधायी प्राथमिकताओं और एजेंडा को साझा करती है।
रिजिजू का यह बयान कि “संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है”, सर्वदलीय बैठक के महत्व को रेखांकित करता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार और विपक्ष दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और सार्थक बहस के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें।
संसदीय कार्यप्रणाली में चुनौतियां:
भारतीय संसद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं:
- लगातार व्यवधान: अक्सर विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और व्यवधानों के कारण संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। इससे महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाते और जरूरी बहसें अधूरी रह जाती हैं।
- बहस की गुणवत्ता में कमी: कई बार शोरगुल और नारेबाजी के कारण गंभीर बहस की जगह आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं।
- अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता: जब संसद सत्र में नहीं होती, तो सरकार अध्यादेशों का सहारा लेती है। यह संसदीय प्रक्रिया को कमजोर करता है क्योंकि अध्यादेशों पर सदन में पूरी बहस नहीं हो पाती।
- समितियों की भूमिका में कमी: विधेयकों को अक्सर स्थायी समितियों के पास भेजे बिना ही पारित कर दिया जाता है, जिससे उनकी गहन जांच और परामर्श की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- कोरम की कमी: कई बार सदन चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या (कोरम) भी पूरी नहीं होती, जिससे बैठकें रद्द करनी पड़ती हैं।
संसदीय मर्यादाएं और सुचारु संचालन के लिए उपाय:
- नियमों का पालन: सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना।
- सार्थक संवाद: सरकार और विपक्ष के बीच खुला और सार्थक संवाद बनाए रखना।
- सहिष्णुता और सम्मान: विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान बनाए रखना।
- मुद्दों पर ध्यान: व्यक्तिगत हमलों से बचकर जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।
- पीठासीन अधिकारी की भूमिका: लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की निष्पक्ष और दृढ़ भूमिका सदन की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है।
पहलगाम-सीजफायर जैसे मुद्दे पर संसद में रचनात्मक बहस होना आवश्यक है। यह न केवल सरकार को जवाबदेह ठहराएगा, बल्कि नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित भी करेगा। रिजिजू का बयान इसी दिशा में एक आह्वान है – कि सदन राजनीतिक अखाड़ा न बनकर, राष्ट्र निर्माण का मंच बना रहे।
राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक चुनौतियां: जम्मू-कश्मीर का संदर्भ
पहलगाम विवाद जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील सुरक्षा परिदृश्य में आता है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करती है। भारत के लिए जम्मू-कश्मीर हमेशा से एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र रहा है, जिसकी सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।
जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियां:
- सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और घुसपैठ जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी चुनौती रही है। आतंकवादी समूह लगातार भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं।
- स्थानीय उग्रवाद: सीमा पार से समर्थन के अलावा, जम्मू-कश्मीर में स्थानीय उग्रवाद भी एक गंभीर चिंता का विषय रहा है, हालांकि धारा 370 के निरस्त होने के बाद इसमें कमी देखी गई है।
- नारको-टेररिज्म: नशीले पदार्थों की तस्करी का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, जिससे एक दोहरा खतरा पैदा हो रहा है।
- साइबर युद्ध और दुष्प्रचार: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलगाववादी भावनाओं को भड़काने और गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया जाता है।
- सामान्य जनजीवन पर प्रभाव: निरंतर सुरक्षा चुनौतियों का क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन और सामान्य जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
धारा 370 के निरस्त होने के बाद का परिदृश्य:
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, सरकार ने क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।
- सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई मौजूदगी: क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सघन तैनाती जारी है ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को रोका जा सके।
- विकास पर जोर: सरकार का ध्यान अब क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर है, ताकि स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में लाया जा सके।
- स्थानीय निकाय चुनावों की बहाली: पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों।
- मानवाधिकारों का संतुलन: सुरक्षा अभियानों के दौरान मानवाधिकारों के सम्मान को बनाए रखना एक नाजुक संतुलन है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और घरेलू स्तर पर भी ध्यान दिया जाता है।
पहलगाम-सीजफायर विवाद का सुरक्षा निहितार्थ:
यदि विपक्ष का आरोप किसी विशिष्ट सुरक्षा चूक या नीतिगत बदलाव से संबंधित है, तो इसके गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं:
- यह सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।
- यह सीमा पार के तत्वों को गलत संदेश भेज सकता है।
- यह क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकता है।
इसलिए, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट और निर्णायक जवाब दे, ताकि किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा एक गैर-पक्षपातपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, जहां राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही इसे सुनिश्चित करने की कुंजी है।
आगे की राह: सशक्त लोकतंत्र की ओर
पहलगाम-सीजफायर विवाद, आगामी मानसून सत्र और संसद के संचालन पर संसदीय कार्य मंत्री के बयान का यह पूरा प्रकरण भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को उजागर करता है। एक सशक्त और कार्यकुशल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कदम महत्वपूर्ण हैं:
- संसदीय संवाद को प्राथमिकता: संसद को सार्थक बहस का मंच बनाए रखना सर्वोपरि है। सरकार और विपक्ष दोनों को संसदीय नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। व्यवधानों के बजाय बहस और चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पर सर्वसम्मति: राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर संवेदनशील जानकारी साझा करनी चाहिए (जितना राष्ट्रीय हित में संभव हो)। विपक्ष को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामलों में गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने से बचना चाहिए।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और जनता तथा संसद के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। समय पर और स्पष्ट जानकारी साझा करने से अफवाहों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगता है।
- विपक्ष की रचनात्मक भूमिका: विपक्ष को न केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, बल्कि वैकल्पिक समाधान और नीतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। उनका विरोध तर्कसंगत, तथ्यों पर आधारित और संवैधानिक होना चाहिए।
- मीडिया की जिम्मेदार भूमिका: मीडिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के सटीक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और सार्वजनिक बहस में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचकर गहन विश्लेषण पर जोर देना चाहिए।
- नागरिकों की भागीदारी: नागरिकों को भी संसदीय कार्यवाही और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों पर सार्थक बहस के लिए दबाव डालना चाहिए।
“लोकतंत्र की शक्ति उसके वाद-विवाद में निहित है, न कि उसके व्यवधानों में। जब बहस रुक जाती है, तो प्रगति भी रुक जाती है।”
यह आवश्यक है कि सभी हितधारक – सरकार, विपक्ष, संसद सदस्य, मीडिया और नागरिक – अपनी-अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारी से निभाएं। पहलगाम-सीजफायर मुद्दा एक अवसर प्रदान करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय मर्यादा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिंतन और सार्वजनिक बहस हो, जिससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत बन सके। आगामी मानसून सत्र न केवल विधायी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह इस बात की भी परीक्षा होगी कि हमारे राजनेता कितनी परिपक्वता के साथ राष्ट्रीय हित के मुद्दों को सुलझाते हैं।
UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
- प्रश्न 1: भारतीय संसदीय प्रणाली में सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह संसद सत्र शुरू होने से पहले बुलाई जाती है ताकि आगामी सत्र के एजेंडा पर चर्चा की जा सके।
- इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है।
- यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित एक प्रावधान है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल a
(B) केवल a और b
(C) केवल b और c
(D) a, b और c
उत्तर: (A) केवल a
व्याख्या: सर्वदलीय बैठकें संसद सत्र शुरू होने से पहले आगामी सत्र के एजेंडा और सुचारु संचालन पर चर्चा के लिए बुलाई जाती हैं। इसकी अध्यक्षता आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री या प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है, न कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा। यह एक संसदीय परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान नहीं।
- प्रश्न 2: भारतीय संसद के संदर्भ में, ‘प्रश्नकाल’ (Question Hour) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा होता है।
- इसमें संसद सदस्य मंत्रियों से सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछते हैं।
- प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प-सूचना प्रश्न।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल a और b
(B) केवल b और c
(C) केवल a और c
(D) a, b और c
उत्तर: (D) a, b और c
व्याख्या: प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा (सुबह 11 बजे से 12 बजे तक) होता है, जिसमें सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित (मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न), अतारांकित (लिखित उत्तर, कोई पूरक प्रश्न नहीं), और अल्प-सूचना प्रश्न (10 दिन से कम के नोटिस पर पूछे गए)।
- प्रश्न 3: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 109
(B) अनुच्छेद 110
(C) अनुच्छेद 245
(D) अनुच्छेद 246
उत्तर: (C) अनुच्छेद 245
व्याख्या: अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। यह संसद को भारत के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 246 विधायी विषयों के वितरण (संघ, राज्य और समवर्ती सूची) से संबंधित है।
- प्रश्न 4: जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने वाला अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया था?
(A) 5 अगस्त 2019
(B) 26 जनवरी 2020
(C) 15 अगस्त 2019
(D) 31 अक्टूबर 2019
उत्तर: (A) 5 अगस्त 2019
व्याख्या: भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया।
- प्रश्न 5: भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?
- विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को बिना किसी अपवाद के समर्थन देना है।
- यह सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विपक्ष वैकल्पिक नीतियों और विचारों को प्रस्तुत कर सकता है।
सही नहीं है/हैं?
(A) केवल a
(B) केवल b
(C) केवल a और c
(D) b और c
उत्तर: (A) केवल a
व्याख्या: विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और कार्यों की निगरानी करना, आलोचना करना और उसे जवाबदेह ठहराना है, न कि बिना किसी अपवाद के समर्थन देना। वे वैकल्पिक नीतियां और विचार भी प्रस्तुत करते हैं।
- प्रश्न 6: भारतीय संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- यदि यह पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल a और b
(B) केवल b और c
(C) केवल a और c
(D) a, b और c
उत्तर: (D) a, b और c
व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसे स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यदि यह पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
- प्रश्न 7: भारत में संसदीय कार्यवाही में ‘शून्यकाल’ (Zero Hour) के बारे में सही कथन चुनें:
(A) यह प्रश्नकाल से पहले होता है।
(B) यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया का एक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हिस्सा है।
(C) इस दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं।
(D) इस पर बहस के लिए 30 मिनट का निश्चित समय आवंटित किया जाता है।
उत्तर: (C) इस दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं।
व्याख्या: शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है। यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया में एक अनौपचारिक नवाचार है, जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठाते हैं। इसका कोई निश्चित समय आवंटित नहीं होता, यह तब तक चलता है जब तक अध्यक्ष अनुमति देते हैं।
- प्रश्न 8: भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) निम्नलिखित में से किस स्थिति में बुलाई जा सकती है?
(A) धन विधेयक पर असहमति होने पर
(B) संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति होने पर
(C) सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर
(D) उपरोक्त सभी
उत्तर: (C) सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर
व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) पर लोकसभा का वर्चस्व होता है और राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रश्न 9: भारत की संसद में एक विधेयक को कानून बनने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
- पहला पठन (First Reading)
- दूसरा पठन (Second Reading)
- समिति चरण (Committee Stage)
- तीसरा पठन (Third Reading)
- राष्ट्रपति की स्वीकृति (President’s Assent)
सही क्रम का चयन करें:
(A) i, ii, iii, iv, v
(B) i, iii, ii, iv, v
(C) ii, i, iii, iv, v
(D) i, ii, iv, iii, v
उत्तर: (A) i, ii, iii, iv, v
व्याख्या: एक विधेयक को कानून बनने के लिए आम तौर पर पांच चरणों से गुजरना पड़ता है: पहला पठन (परिचय), दूसरा पठन (सामान्य चर्चा और विस्तृत जांच, जिसमें समिति चरण शामिल हो सकता है), तीसरा पठन (केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना), दूसरे सदन में पारित होना, और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति। समिति चरण आमतौर पर दूसरे पठन के दौरान या उसके बाद आता है।
- प्रश्न 10: ‘नियंत्रण रेखा’ (Line of Control – LoC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते के तहत स्थापित की गई थी।
- यह जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो दोनों देशों के सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल a और b
(B) केवल b और c
(C) केवल a और c
(D) a, b और c
उत्तर: (B) केवल b और c
व्याख्या: LoC भारत और पाकिस्तान के बीच एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यह 1971 के युद्ध के बाद 1972 के शिमला समझौते के तहत स्थापित की गई थी, जो पूर्व सीजफायर लाइन का नया नाम है। यह दोनों देशों के सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को जम्मू-कश्मीर में अलग करती है।
मुख्य परीक्षा (Mains)
- “राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की रचनात्मक भूमिका एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।” पहलगाम-सीजफायर विवाद के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और बताएं कि कैसे संसदीय मर्यादाएं इस प्रक्रिया को मजबूत कर सकती हैं।
- भारतीय संसद के समक्ष वर्तमान समय में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? इन चुनौतियों का सामना करने और संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुधार सुझाएंगे?
- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने में भारत को किन आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद के प्रभावों का मूल्यांकन करें।