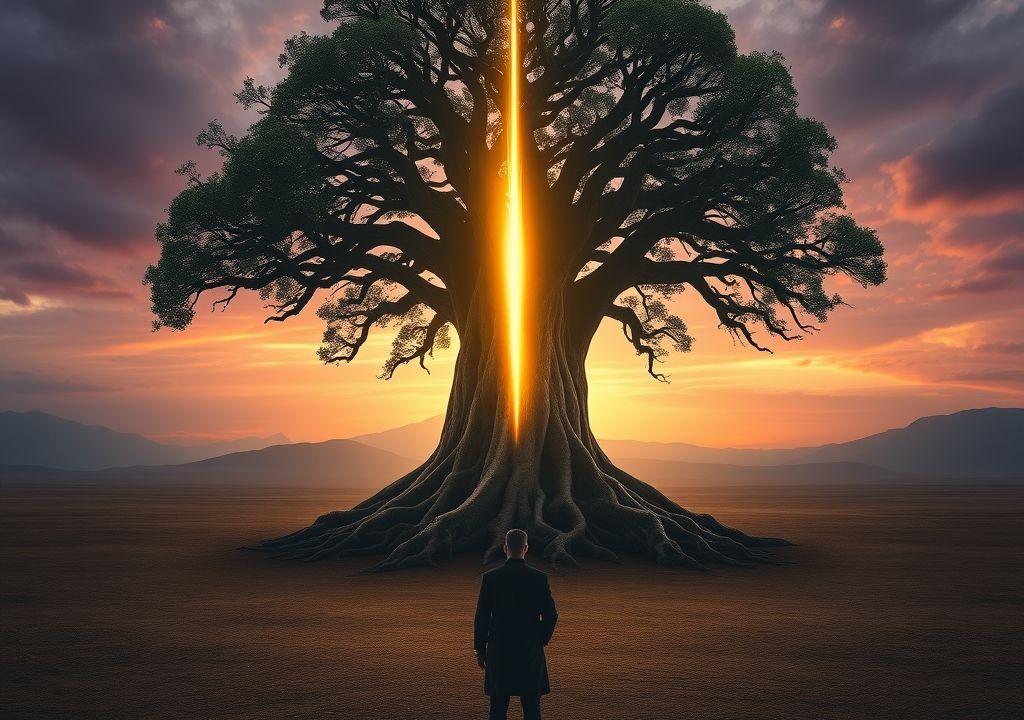थरूर की दृढ़ता: जब देशहित पार्टी के अनुशासन पर भारी पड़े – एक गहन विश्लेषण
चर्चा में क्यों? (Why in News?):
हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तित्व शशि थरूर ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करने के बावजूद, उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि उनके लिए ‘देश पहले, पार्टी बाद में’ है। यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत दर्शन को दर्शाता है, बल्कि यह लोकतंत्र में व्यक्तिगत विवेक, पार्टी अनुशासन और राष्ट्रीय हित के बीच के जटिल संबंध पर भी प्रकाश डालता है। यह मुद्दा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह शासन, नैतिकता, भारतीय राजनीति और संविधान से जुड़े कई आयामों को छूता है। आइए इस बयान के गहरे निहितार्थों और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को गहराई से समझें।
व्यक्तिगत निष्ठा बनाम दलगत अनुशासन: एक शाश्वत द्वंद्व
लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। वे विचारधाराओं को संगठित करते हैं, नीतियों को आकार देते हैं, चुनावों में प्रतिस्पर्धा करते हैं और शासन करते हैं। इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दलगत अनुशासन (Party Discipline) अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी के सदस्य एक साझा उद्देश्य के लिए काम करें, एकजुट होकर नीतियों का समर्थन करें और सरकार चलाने या विपक्ष की भूमिका निभाने में स्थिरता प्रदान करें। एक मजबूत पार्टी लाइन के बिना, नीतियां खंडित हो सकती हैं, और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू व्यक्तिगत निष्ठा (Individual Loyalty) और विवेक (Conscience) है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपनी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता, बल्कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र और अंततः पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब पार्टी का रुख व्यक्तिगत नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों या व्यापक राष्ट्रीय हित के साथ संघर्ष कर सकता है। ऐसे में, एक नेता को कहाँ अपनी निष्ठा रखनी चाहिए – पार्टी के प्रति या देश के प्रति?
कल्पना कीजिए एक जहाज का। पार्टी अनुशासन वह इंजन और पतवार है जो जहाज को एक निश्चित दिशा में ले जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि जहाज अपनी गति और दिशा बनाए रखे। लेकिन जहाज का वास्तविक लक्ष्य यात्रियों (जनता) को सुरक्षित और कुशलता से गंतव्य (राष्ट्रीय हित) तक पहुँचाना है। यदि जहाज का कप्तान (पार्टी नेतृत्व) जहाज को किसी खतरे (जनविरोधी नीति) की ओर ले जा रहा है, तो चालक दल के सदस्य (पार्टी सदस्य) का प्राथमिक कर्तव्य जहाज और उसमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो जाता है, भले ही इसके लिए कप्तान के आदेशों से असहमति व्यक्त करनी पड़े। शशि थरूर का बयान इसी द्वंद्व को सामने लाता है।
शशि थरूर का बयान: ‘मेरे लिए देश पहले, पार्टी बाद में’ का निहितार्थ
यह बयान भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जहां जनता की संप्रभुता सर्वोपरि है। इसके कई गहरे निहितार्थ हैं:
- प्रतिनिधि का सर्वोच्च कर्तव्य: यह याद दिलाता है कि एक निर्वाचित सांसद या विधायक का प्राथमिक कर्तव्य अपने मतदाताओं और देश के प्रति है, न कि केवल अपनी पार्टी के प्रति।
- नैतिकता और विवेक की प्रधानता: यह राजनीति में नैतिक निर्णय लेने और व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि यदि पार्टी लाइन राष्ट्रहित के खिलाफ जाती है, तो नेता को नैतिक साहस दिखाना चाहिए।
- पार्टी प्रणाली की आलोचना: यह अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, जहाँ अक्सर व्यक्तिगत विचारों और आंतरिक लोकतंत्र के लिए बहुत कम जगह होती है।
- संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा: यह संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसमें व्यक्ति को संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, भले ही यह पार्टी के दबाव के विपरीत हो।
- सार्थक बहस का आह्वान: यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक सार्थक असहमति और बहस को बढ़ावा देने का आह्वान है, जहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान किया जाता है।
गांधीजी ने एक बार कहा था, “मेरी देशभक्ति सर्व समावेशी है और मैं अन्य देशों की देशभक्ति को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने देश को सिर्फ इसलिए बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ, ताकि मैं दूसरे देशों को नुकसान पहुँचा सकूँ।” यह दर्शाता है कि राष्ट्रहित की अवधारणा किसी भी संकीर्ण विचारधारा या दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।
भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण और असहमति की भूमिका
भारतीय राजनीतिक इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ नेताओं ने दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में अपनी बात रखी है।
- लाल बहादुर शास्त्री: रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना, यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और जवाबदेही दलगत राजनीति से ऊपर है।
- मोरारजी देसाई: उन्होंने अपनी ही पार्टी के भीतर कई नीतियों पर खुलकर असहमति व्यक्त की, जिसे अक्सर उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है।
- कई क्षेत्रीय नेताओं का उदय: अक्सर स्थापित राष्ट्रीय दलों की नीतियों से असहमति या उनके द्वारा अनदेखी महसूस करने के परिणामस्वरूप हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगे।
लोकतंत्र में असहमति (Dissent) की भूमिका:
असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्राण है। यह केवल विरोध नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि:
- निरंकुशता पर अंकुश: बहुमत की निरंकुशता को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि सभी आवाजों को सुना जाए।
- नीतियों में सुधार: आलोचना और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से नीतियों में सुधार और परिष्करण संभव होता है।
- नवाचार को बढ़ावा: स्थापित मानदंडों को चुनौती देकर नए विचारों और समाधानों को जन्म देता है।
- जवाबदेही सुनिश्चित: नेताओं और सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
- राष्ट्रीय एकता: विभिन्न समुदायों और विचारों को एक साथ लाता है, जिससे व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनती है।
हालांकि, रचनात्मक असहमति और केवल विरोध के लिए विरोध के बीच एक बारीक रेखा होती है। रचनात्मक असहमति का उद्देश्य समाधान खोजना होता है, जबकि केवल विरोध का उद्देश्य अक्सर राजनीतिक लाभ होता है।
चुनौतियाँ और जोखिम
शशि थरूर जैसे बयान देना या दलगत लाइन से हटकर खड़ा होना आसान नहीं होता है। इसके साथ कई चुनौतियाँ और जोखिम जुड़े होते हैं:
- पार्टी से निष्कासन/अनुशासनात्मक कार्रवाई: अक्सर ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया जाता है।
- राजनीतिक अलगाव: असंतुष्ट नेता को पार्टी और उसके समर्थकों द्वारा अलग-थलग किया जा सकता है।
- दलबदल कानून का खतरा: भारत में दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) ने पार्टी व्हिप के उल्लंघन को हतोत्साहित किया है, जिससे नेताओं के लिए अपनी राय व्यक्त करना और भी मुश्किल हो गया है। हालाँकि, यह कानून मूल रूप से विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए बनाया गया था, न कि रचनात्मक असहमति को रोकने के लिए।
- अवसरवादी होने का आरोप: ऐसे नेता पर अक्सर अवसरवादी होने या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करने का आरोप लगाया जा सकता है।
- पार्टी के भीतर विभाजन: बार-बार की असहमति पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और विभाजन को जन्म दे सकती है, जिससे उसकी एकजुटता कमजोर होती है।
यह महत्वपूर्ण है कि दलगत अनुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित किया जाए। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन साथ ही पार्टी के सामूहिक निर्णयों का सम्मान भी करें, आदर्श मानी जाती है।
आगे की राह: संतुलन कैसे स्थापित करें?
एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के लिए, दलगत अनुशासन और व्यक्तिगत विवेक के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
-
पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा:
- पार्टियों को अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बहस करने और अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उन्हें यह महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है।
-
दलबदल विरोधी कानून की समीक्षा:
- इस कानून का उद्देश्य दल-बदल को रोकना था, न कि रचनात्मक असहमति को दबाना।
- विशेषज्ञों द्वारा इस कानून की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विधायकों को राष्ट्रीय हित में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से न रोके।
-
नैतिक नेतृत्व का विकास:
- राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि उनका प्राथमिक कर्तव्य राष्ट्र और उसके नागरिकों के प्रति है।
- नैतिकता और मूल्यों को राजनीति के केंद्र में लाना चाहिए।
-
नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका:
- जागरूक नागरिक समाज और स्वतंत्र मीडिया असहमति के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं और नेताओं को उनकी जवाबदेही के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- वे दलगत दबावों से परे जाकर राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उजागर कर सकते हैं।
-
जागरूक मतदाता:
- मतदाताओं को ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी की आलोचना झेलनी पड़े।
- राजनीतिक दलों को सिर्फ ‘पार्टी लाइन’ के आधार पर नहीं, बल्कि उनके राष्ट्र हित में लिए गए निर्णयों के आधार पर भी आंका जाना चाहिए।
निष्कर्ष
शशि थरूर का ‘देश पहले, पार्टी बाद में’ का बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। यह एक ऐसे राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर देता है जहाँ व्यक्तिगत विवेक, संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्रीय हित को दलगत निष्ठा और अनुशासन से ऊपर रखा जाए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, असहमति को केवल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बशर्ते वह रचनात्मक हो और राष्ट्रहित की भावना से प्रेरित हो। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, को ऐसे सिद्धांतों को बनाए रखना और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उसके नेता वास्तविक अर्थों में जनता के सेवक बन सकें और देश के व्यापक हित में कार्य कर सकें। अंततः, किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व देश के अस्तित्व पर निर्भर करता है, और यदि देश की नींव मजबूत है, तो ही दल सशक्त हो सकते हैं।
UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs
1. शशि थरूर के ‘देश पहले, पार्टी बाद में’ के बयान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
2. यह लोकतांत्रिक शासन में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को रेखांकित करता है।
3. यह दलबदल विरोधी कानून के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रत्यक्ष कारण बन सकता है यदि यह पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (d)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें राजनेताओं द्वारा अपनी राय व्यक्त करना भी शामिल है।
- कथन 2 सही है: यह बयान स्पष्ट रूप से नैतिक निर्णय लेने और व्यक्तिगत विवेक को दलगत निष्ठा से ऊपर रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
- कथन 3 सही है: यदि किसी पार्टी सदस्य का बयान या कार्य पार्टी के आधिकारिक रुख या व्हिप का उल्लंघन करता है, तो दलबदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहाँ तक कि सदन की सदस्यता रद्द करने का आधार भी बन सकता है, हालांकि यह बयान स्वयं व्हिप का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या पार्टी विरोधी गतिविधि के रूप में की जा सकती है।
2. दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
2. यह कानून केवल सांसदों पर लागू होता है, विधायकों पर नहीं।
3. एक मनोनीत सदस्य सदन में शामिल होने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, बिना दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं।
- कथन 2 गलत है: यह कानून सांसदों (संसद सदस्यों) और विधायकों (राज्य विधानमंडल सदस्यों) दोनों पर लागू होता है।
- कथन 3 गलत है: एक मनोनीत सदस्य सदन में शामिल होने के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। यदि वह 6 महीने के बाद शामिल होता है, तो उसे दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।
3. ‘व्हिप’ (Whip) शब्द के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से इसकी भूमिका का वर्णन करता है?
(a) यह एक संसदीय उपकरण है जो सदस्यों को सदन में बिल पर मतदान करने के लिए मजबूर करता है।
(b) यह एक राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश है, जिसमें पार्टी सदस्यों को सदन में एक निश्चित तरीके से मतदान करने या उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।
(c) यह विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक साधन है।
(d) यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया आदेश है।
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
व्याख्या:
एक व्हिप एक राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया लिखित आदेश है, जिसमें उसके सदस्यों को सदन में किसी विशेष मुद्दे पर मतदान करने या उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।
4. भारतीय लोकतंत्र में ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह संविधान के सिद्धांतों को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का विचार है।
2. यह अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में विकसित की गई है।
3. यह व्यक्तिगत विवेक को पार्टी के रुख पर प्राथमिकता देने को प्रोत्साहित करता है, जब दोनों में टकराव हो।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (d)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान के मूल मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखना है, चाहे दलगत हित कुछ भी हों।
- कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संवैधानिक नैतिकता’ की अवधारणा को विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों, जैसे कि सबरीमाला मामले, में विकसित और प्रयोग किया है।
- कथन 3 सही है: संवैधानिक नैतिकता व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही यह पार्टी के रुख के विपरीत हो, विशेषकर यदि पार्टी का रुख संविधान के मूल्यों से विचलन करता हो।
5. भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनकी आंतरिक लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है?
1. पार्टी अध्यक्षों का बार-बार चुनाव न होना।
2. प्रमुख निर्णयों में शीर्ष नेतृत्व का अत्यधिक प्रभाव।
3. पार्टी व्हिप का अत्यधिक उपयोग।
4. पार्टी सदस्यों के लिए अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अभाव।
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (d)
व्याख्या: उपरोक्त सभी बिंदु भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को दर्शाते हैं। पार्टी अध्यक्षों का नियमित चुनाव न होना, शीर्ष नेतृत्व द्वारा सभी प्रमुख निर्णय लेना, पार्टी व्हिप का अत्यधिक उपयोग जिससे सदस्यों की व्यक्तिगत राय दब जाती है, और सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अभाव, ये सभी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमजोरी के संकेतक हैं।
6. निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘राष्ट्र हित’ (National Interest) की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?
(a) यह सत्तारूढ़ दल की नीतियों और कार्यक्रमों का समूह है।
(b) यह किसी देश की दीर्घकालिक सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण के लिए सबसे अच्छा माना जाने वाला उद्देश्य है।
(c) यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र की शक्ति और प्रभाव का माप है।
(d) यह किसी विशेष सांस्कृतिक या भाषाई समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
व्याख्या: राष्ट्र हित एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश की सामूहिक भलाई, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि को संदर्भित करती है। यह किसी एक पार्टी या समूह के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की भलाई से संबंधित है।
7. भारतीय संसदीय प्रणाली में ‘व्हिप’ जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) सदन में मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
(b) संसदीय कार्यवाही का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
(c) पार्टी सदस्यों के बीच मतदान में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना।
(d) विपक्ष को सदन में बहस करने से रोकना।
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
व्याख्या: व्हिप का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सभी सदस्य महत्वपूर्ण मतदान के दौरान एकजुट होकर कार्य करें और पार्टी लाइन का पालन करें, जिससे पार्टी के भीतर अनुशासन और स्थिरता बनी रहे।
8. भारत में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के संबंध में, उसका प्राथमिक कर्तव्य किसके प्रति होता है?
1. अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रति
2. अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति
3. भारत के संविधान के प्रति
4. सरकार में अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति
निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें:
(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
व्याख्या: एक निर्वाचित प्रतिनिधि का प्राथमिक कर्तव्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और भारत के संविधान के प्रति होता है। जबकि उसे अपनी पार्टी के प्रति भी निष्ठा रखनी होती है, लेकिन संवैधानिक मूल्य और जनता का हित हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर होने चाहिए। सरकार में वरिष्ठ नेताओं के प्रति निष्ठा भी आवश्यक है, लेकिन वह संवैधानिक और सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं हो सकती।
9. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वस्थ लोकतंत्र में ‘रचनात्मक असहमति’ (Constructive Dissent) की विशेषता नहीं है?
(a) इसका उद्देश्य मौजूदा नीतियों या विचारों में सुधार लाना होता है।
(b) यह अक्सर गहन विचार-विमर्श और साक्ष्य-आधारित तर्क पर आधारित होता है।
(c) इसका मुख्य उद्देश्य सरकार या पार्टी को कमजोर करना होता है।
(d) यह विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए जगह बनाता है और खुले संवाद को बढ़ावा देता है।
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
व्याख्या: रचनात्मक असहमति का उद्देश्य प्रणाली को बेहतर बनाना है, न कि उसे कमजोर करना। इसका लक्ष्य नीतियों, निर्णयों या विचारों में सुधार लाना, उन्हें अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है। सरकार या पार्टी को कमजोर करना आमतौर पर रचनात्मक असहमति का नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध या विध्वंसक गतिविधियों का लक्ष्य होता है।
10. संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है?
(a) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण
(b) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
(c) संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के दलबदल के आधार पर अयोग्यता
(d) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
व्याख्या: संविधान की दसवीं अनुसूची (52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई) संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा (Mains)
1. “संसदीय लोकतंत्र में दलगत अनुशासन आवश्यक है, लेकिन यह व्यक्तिगत विवेक और राष्ट्र हित की कीमत पर नहीं होना चाहिए।” शशि थरूर के हालिया बयान के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (Approx. 250 शब्द)
2. भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, नेताओं को ‘देश पहले, पार्टी बाद में’ जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करने में कैसे बाधा डालती है? इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? (Approx. 250 शब्द)
3. ‘दलबदल विरोधी कानून’ को अक्सर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने वाला बताया जाता है। क्या यह कानून ‘रचनात्मक असहमति’ के लिए जगह छोड़ता है? भारतीय लोकतंत्र में ‘रचनात्मक असहमति’ की भूमिका का मूल्यांकन करें। (Approx. 250 शब्द)
4. “नैतिकता और शासन एक दूसरे के पूरक हैं।” शशि थरूर के ‘देश पहले’ बयान के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें और चर्चा करें कि कैसे नैतिक नेतृत्व सुशासन में योगदान कर सकता है। (Approx. 250 शब्द)