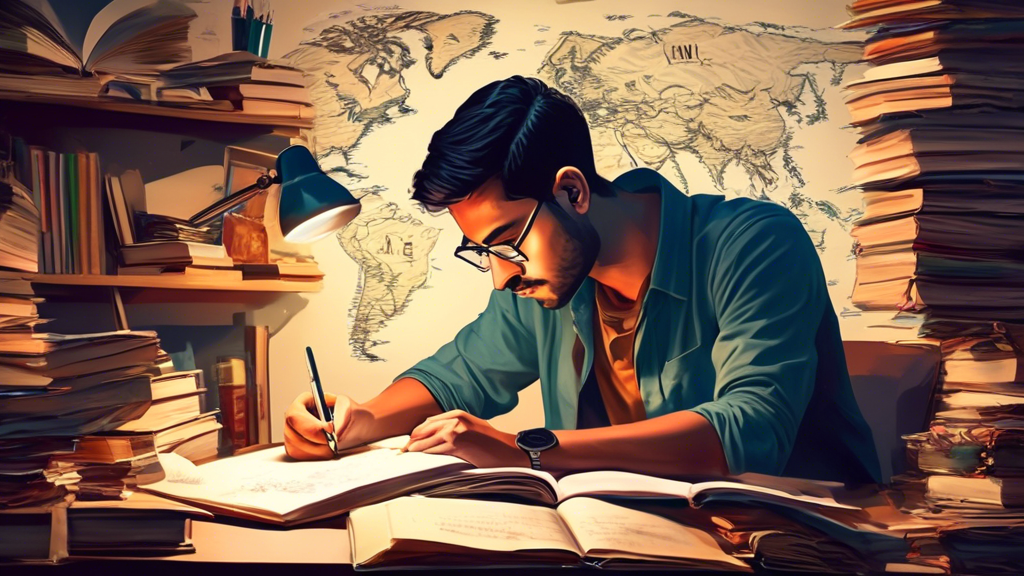UPSC गाइड: यूपी और J&K में ‘ऑरेंज अलर्ट’ के बीच भारी बारिश, बादल फटने का खतरा – जानें पूरी कहानी और प्रभाव
चर्चा में क्यों? (Why in News?):
हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने (Cloudburst) जैसी घटनाओं का खतरा भी बताया गया है। यह अलर्ट न केवल आम जनजीवन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और समसामयिक घटनाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए, इस स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करें और समझें कि यह हमारे देश के लिए और हमारी परीक्षा के लिए क्या मायने रखती है।
जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं का बढ़ता खतरा (Climate Change and the Rising Threat of Extreme Weather Events)
हाल के वर्षों में, भारत सहित दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। बेमौसम बारिश, तीव्र लू, असामान्य रूप से ठंडी सर्दियाँ, और विनाशकारी बाढ़ जैसी घटनाएँ अब “नया सामान्य” बनती जा जा रही हैं। यह सीधे तौर पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में होने वाले जटिल परिवर्तनों से जुड़ा है।
यह स्थिति हमें न केवल तत्काल राहत और बचाव उपायों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि दीर्घकालिक अनुकूलन (Adaptation) और शमन (Mitigation) रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाती है। UPSC के दृष्टिकोण से, यह विषय बहुआयामी है, जिसमें भूगोल (मानसून, वर्षा के पैटर्न), पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन के प्रभाव), आपदा प्रबंधन (तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास), और शासन (नीति निर्माण, अंतर-राज्यीय समन्वय) जैसे कई पहलू शामिल हैं।
आईएमडी का रंग-कोडित अलर्ट सिस्टम क्या है? (What is IMD’s Color-Coded Alert System?)
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मौसम संबंधी खतरों के प्रति जनता और सरकारी एजेंसियों को सचेत करने के लिए एक रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली का उपयोग करता है। यह प्रणाली संभावित जोखिमों की गंभीरता को दर्शाती है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देती है। इसे समझना महत्वपूर्ण है, खासकर आपदा प्रबंधन के संदर्भ में।
- ग्रीन अलर्ट (Green Alert): “सब ठीक है” या “कोई चेतावनी नहीं”। इसका मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य है और कोई विशेष खतरा नहीं है।
- येलो अलर्ट (Yellow Alert): “देखें और अपडेट रहें” या “सावधान रहें”। यह संकेत देता है कि खराब मौसम की संभावना है जो सामान्य गतिविधियों को बाधित कर सकती है। इसमें जनता को जागरूक और तैयार रहने की सलाह दी जाती है।
- ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): “तैयार रहें” या “खतरनाक मौसम”। यह चेतावनी गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत देती है जो जीवन और संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें सरकारी एजेंसियों को तैयार रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में यात्रा से बचना या सुरक्षित आश्रय में रहना महत्वपूर्ण होता है।
- रेड अलर्ट (Red Alert): “कार्य करें” या “अत्यंत खतरनाक मौसम”। यह सबसे गंभीर चेतावनी है, जो बताती है कि अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति लगभग निश्चित है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान और क्षति हो सकती है। इसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जैसे निकासी या आपातकालीन आश्रयों में जाना।
वर्तमान स्थिति में, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ का मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जो बाढ़, जलजमाव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है।
भारी बारिश और बादल फटना: क्या अंतर है? (Heavy Rain and Cloudburst: What’s the Difference?)
ये दोनों ही शब्द अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना आवश्यक है।
भारी बारिश (Heavy Rain)
भारी बारिश एक सामान्य मौसमी घटना है जिसमें अपेक्षाकृत लंबी अवधि में बड़ी मात्रा में वर्षा होती है। IMD के अनुसार, 24 घंटे की अवधि में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच वर्षा को ‘भारी वर्षा’ माना जाता है, जबकि 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक ‘बहुत भारी वर्षा’ और 204.5 मिमी से अधिक ‘अत्यंत भारी वर्षा’ कहलाती है।
विशेषताएँ:
- समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होती है।
- बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकती है।
- आमतौर पर मानसूनी गतिविधियों या पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी होती है।
- बाढ़, जलभराव का कारण बन सकती है।
बादल फटना (Cloudburst)
बादल फटना एक अत्यंत स्थानीयकृत और तीव्र वर्षा की घटना है। IMD के अनुसार, यदि एक घंटे की अवधि में 20 मिमी या उससे अधिक वर्षा होती है, और यह घटना एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र (20-30 वर्ग किलोमीटर) तक सीमित होती है, तो उसे बादल फटना माना जाता है। हालाँकि, कुछ परिभाषाएँ 100 मिमी प्रति घंटे की दर को भी मानती हैं।
विशेषताएँ:
- अत्यंत तीव्र और अचानक होती है।
- बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है।
- अक्सर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है।
- अक्सर संवहन धाराओं (Convective Currents) और तीव्र ऊपर उठती हवा (Updrafts) के कारण होती है, जो बादलों में बड़ी मात्रा में पानी जमा कर देती है, और जब ये बादल इसे धारण नहीं कर पाते, तो यह एक साथ नीचे गिर जाता है।
- परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ (Flash Floods), भूस्खलन और मलबे का प्रवाह (Debris Flow) होता है, जो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं।
- इसकी भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत स्थानीयकृत घटना है।
वर्तमान अलर्ट में जम्मू-कश्मीर में बादल फटने का खतरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी और भूस्खलन-प्रवण है, जहाँ ऐसी घटनाएँ गंभीर परिणाम दे सकती हैं, जैसा कि हमने अतीत में केदारनाथ (उत्तराखंड) और लेह (लद्दाख) जैसी आपदाओं में देखा है।
इन मौसमी घटनाओं के कारण (Causes of These Weather Events)
भारत में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएँ कई कारकों के संयोजन से होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
1. दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता (Active Southwest Monsoon)
भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है। जब मानसून की अक्षीय रेखा (Monsoon Trough) अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक जाती है, या जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पर्याप्त नमी वाली हवाएँ सक्रिय होती हैं, तो मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय की तलहटी और उत्तर-पूर्वी राज्य विशेष रूप से मानसूनी बारिश के लिए जाने जाते हैं।
2. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances – WDs)
ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ये आमतौर पर सर्दियों में वर्षा लाते हैं, लेकिन कभी-कभी मानसून के मौसम में भी ये पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवाओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो यह भारी वर्षा, बर्फबारी और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। जम्मू-कश्मीर में बादल फटने का खतरा इसी तरह की अंतःक्रिया का परिणाम हो सकता है।
3. स्थलाकृति (Topography)
पहाड़ी क्षेत्र (जैसे हिमालय) ओरोग्राफिक वर्षा (Orographic Rainfall) के लिए प्रवण होते हैं। जब नमी से भरी हवाएँ पहाड़ों से टकराती हैं और ऊपर उठने को मजबूर होती हैं, तो वे ठंडी होकर संघनित होती हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। संकीर्ण घाटियाँ और तीव्र ढलान बादल फटने की स्थिति में पानी के तेजी से बहने और अचानक बाढ़ में बदलने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।
4. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है।
वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वायुमंडल अधिक नमी धारण कर रहा है। जब यह नमी संघनित होती है, तो यह अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाओं का कारण बन सकती है। ‘एक दिन की अत्यधिक वर्षा’ की घटनाओं में वृद्धि, जिसे ‘रेनबॉम्ब्स’ भी कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है।
यह अप्रत्याशित और तीव्र वर्षा के पैटर्न को जन्म देता है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाएँ अधिक आम हो जाती हैं।
5. स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियाँ (Local Atmospheric Conditions)
गर्म, नम हवा का तेजी से ऊपर उठना (संवहन) और एक छोटे क्षेत्र में बादलों में अत्यधिक नमी का जमा होना बादल फटने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाता है। जब ये बादल बड़ी मात्रा में पानी को धारण नहीं कर पाते, तो यह एक साथ गिर जाता है।
प्रभाव और परिणाम (Impacts and Consequences)
भारी बारिश और बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाओं के दूरगामी और विनाशकारी परिणाम होते हैं, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं।
1. पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impacts)
- बाढ़ और जलभराव (Flooding & Waterlogging): निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है।
- भूस्खलन और मृदा अपरदन (Landslides & Soil Erosion): पहाड़ी क्षेत्रों में, संतृप्त मिट्टी भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे सड़कें, गाँव और बुनियादी ढाँचा नष्ट हो जाते हैं। तीव्र वर्षा मिट्टी के ऊपरी परत को बहा ले जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है।
- नदी के प्रवाह में वृद्धि (Increased River Flow): नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्र और निचले बांधों को खतरा होता है।
- जैव विविधता पर प्रभाव (Impact on Biodiversity): प्राकृतिक आवासों का विनाश, जीवों का विस्थापन और कुछ प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न होता है।
2. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impacts)
- जानमाल का नुकसान (Loss of Life and Property): यह सबसे सीधा और दुखद परिणाम है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाती है और घरों, व्यवसायों और संपत्ति को भारी नुकसान होता है।
- बुनियादी ढाँचे का विनाश (Destruction of Infrastructure): सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें, बिजली के खंभे और संचार प्रणालियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे कनेक्टिविटी टूट जाती है और राहत कार्यों में बाधा आती है।
- कृषि पर प्रभाव (Impact on Agriculture): फसलें पानी में डूब जाती हैं, जिससे भारी फसल का नुकसान होता है। यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है और किसानों की आजीविका छीन लेता है।
- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे (Health Issues): बाढ़ के पानी से जल-जनित बीमारियाँ (जैसे हैजा, टाइफाइड), वेक्टर-जनित बीमारियाँ (जैसे डेंगू, मलेरिया) और त्वचा संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
- आर्थिक नुकसान (Economic Losses): कृषि, पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान होता है। पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर भारी खर्च आता है।
- विस्थापन और आजीविका का नुकसान (Displacement & Loss of Livelihood): हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है। आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक गरीबी और सामाजिक अस्थिरता आती है।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव (Psychological Impact): आपदा के शिकार लोगों में सदमा, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
उदाहरण: उत्तराखंड आपदाएँ
उत्तराखंड में 2013 और उसके बाद की बादल फटने और भारी बारिश की घटनाओं ने इस बात का कड़वा अनुभव दिया है कि कैसे ऐसी आपदाएँ न केवल जानमाल का भारी नुकसान करती हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को दशकों तक प्रभावित करती हैं। चार धाम यात्रा, स्थानीय पर्यटन और कृषि पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है।
भारत की आपदा प्रबंधन संरचना और चुनौतियाँ (India’s Disaster Management Framework & Challenges)
भारत ने आपदाओं से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना की है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 इस ढांचे का आधार है।
प्रमुख संस्थाएँ और उनकी भूमिकाएँ:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशानिर्देश तैयार करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): विशेष रूप से प्रशिक्षित बल जो आपदाओं के दौरान खोज, बचाव और राहत कार्यों में लगे होते हैं।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD): मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने की प्राथमिक एजेंसी।
- केंद्रीय जल आयोग (CWC): बाढ़ पूर्वानुमान और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करता है।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों का समन्वय करता है।
चुनौतियाँ (Challenges):
- पूर्व-चेतावनी प्रणाली की सीमाएँ: बादल फटने जैसी अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए उच्च-रिजॉल्यूशन रडार और उपग्रह डेटा की आवश्यकता होती है।
- बुनियादी ढाँचे का लचीलापन: बढ़ती आबादी और अनियोजित शहरीकरण के कारण बने कमज़ोर बुनियादी ढाँचे (जैसे खराब जल निकासी व्यवस्था, नदी तल पर निर्माण) आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा देते हैं।
- जागरूकता और क्षमता निर्माण: स्थानीय समुदायों, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, आपदाओं के प्रति जागरूकता और प्रतिक्रिया क्षमता का अभाव।
- अंतर-एजेंसी समन्वय: केंद्र और राज्य, विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती है।
- संसाधन की कमी: पर्याप्त धन, प्रशिक्षित कर्मियों और आधुनिक उपकरणों की कमी, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर।
- डेटा प्रबंधन और विश्लेषण: मौसम संबंधी डेटा के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार में सुधार की आवश्यकता।
- जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव: अप्रत्याशित और तीव्र मौसमी घटनाओं के कारण पारंपरिक आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ अपर्याप्त साबित हो रही हैं।
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता का अभाव: विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिससे आपदाओं का जोखिम बढ़ता है।
आगे की राह: तैयारी, अनुकूलन और शमन (Way Forward: Preparedness, Adaptation & Mitigation)
इन चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए एक बहु-आयामी और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास सभी शामिल हों।
1. तैयारी और पूर्व-चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना (Strengthening Preparedness & Early Warning Systems)
- उच्च-रिजॉल्यूशन पूर्वानुमान: IMD की क्षमताओं को और बढ़ाना, विशेष रूप से स्थानीयकृत और तीव्र घटनाओं (जैसे बादल फटना) के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन रडार और मॉडल का उपयोग करके।
- प्रसार तंत्र: चेतावनी संदेशों को अंतिम उपयोगकर्ता तक, विशेषकर दूरदराज और कमजोर क्षेत्रों तक, मोबाइल अलर्ट, रेडियो, टेलीविजन और स्थानीय स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से पहुँचाना।
- मॉक ड्रिल और समुदाय-आधारित तैयारी: नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना और स्थानीय समुदायों को आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना, उन्हें ‘आपदा मित्र’ बनाना।
2. अनुकूलन रणनीतियाँ (Adaptation Strategies)
- जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा: इमारतों, सड़कों, पुलों और जल निकासी प्रणालियों का निर्माण और उन्नयन इस तरह से करना जो चरम मौसम की स्थिति का सामना कर सके। “बिल्डिंग बैक बेटर” के सिद्धांत को अपनाना।
- जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन, जलाशयों का निर्माण, और कुशल सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से पानी के अधिक प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देना। बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण रोकना।
- कृषि अनुकूलन: सूखा-प्रतिरोधी और बाढ़-प्रतिरोधी फसल किस्मों को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना।
- पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण: मैंग्रोव रोपण, वेटलैंड संरक्षण, और वन पुनर्स्थापन के माध्यम से प्राकृतिक बफर को मजबूत करना जो बाढ़ और भूस्खलन के प्रभाव को कम करते हैं।
3. शमन रणनीतियाँ (Mitigation Strategies)
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: पेरिस समझौते और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
- वनीकरण और पुनर्वनीकरण: विशेष रूप से पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सके।
4. शासन और नीतिगत उपाय (Governance and Policy Measures)
- राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन: इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और नियमित रूप से समीक्षा करना।
- भूमि उपयोग नियोजन: बाढ़ संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना।
- अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्यीय समन्वय: विभिन्न सरकारी एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- अनुसंधान और विकास: मौसम विज्ञान, जलवायु मॉडलिंग और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में जारी ‘ऑरेंज अलर्ट’ और बादल फटने का खतरा एक चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और चरम मौसमी घटनाओं के लिए लगातार तैयार रहने की आवश्यकता है। यह केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक जटिल चुनौती है जिसके लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। UPSC उम्मीदवारों के रूप में, हमें इस विषय को न केवल इसके सतही स्तर पर बल्कि इसके गहरे कारणों, प्रभावों और समाधानों के साथ जोड़कर देखना होगा। प्रभावी आपदा प्रबंधन केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, अनुकूलन और दीर्घकालिक लचीलेपन का निर्माण भी शामिल है। भारत को एक ‘आपदा-लचीला’ राष्ट्र बनाने के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, समुदायों और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।
UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs
-
प्रश्न 1: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ‘ऑरेंज अलर्ट’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह चेतावनी गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत देती है जो जीवन और संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है।
- इस अलर्ट का अर्थ है कि मौसम की स्थिति सामान्य है और कोई विशेष खतरा नहीं है।
- यह सरकारी एजेंसियों को तैयार रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3
व्याख्या: ‘ऑरेंज अलर्ट’ गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत देता है और सरकारी एजेंसियों को तैयार रहने तथा लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देता है। ‘मौसम सामान्य है’ का संकेत ग्रीन अलर्ट द्वारा दिया जाता है।
-
प्रश्न 2: ‘बादल फटना’ (Cloudburst) की परिभाषा के संबंध में, IMD के मानदंड के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) 24 घंटे में 20 मिमी से अधिक वर्षा।
(b) एक घंटे में 20 मिमी या उससे अधिक वर्षा, जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो।
(c) 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक वर्षा।
(d) एक घंटे में 10 मिमी से अधिक वर्षा, जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करे।
उत्तर: (b) एक घंटे में 20 मिमी या उससे अधिक वर्षा, जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो।
व्याख्या: IMD ‘बादल फटने’ को एक घंटे की अवधि में 20 मिमी या उससे अधिक वर्षा के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर एक छोटे (20-30 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में होती है।
-
प्रश्न 3: भारत में बादल फटने की घटनाएँ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में अधिक होती हैं?
(a) तटीय मैदान
(b) थार रेगिस्तान
(c) प्रायद्वीपीय पठार
(d) हिमालयी और अन्य पर्वतीय क्षेत्र
उत्तर: (d) हिमालयी और अन्य पर्वतीय क्षेत्र
व्याख्या: बादल फटने की घटनाएँ अक्सर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं जहाँ तीव्र ऊपर उठती हवाएँ और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग बड़ी मात्रा में नमी को बादलों में जमा कर देती हैं, और जब ये बादल इसे धारण नहीं कर पाते, तो यह एक साथ नीचे गिर जाता है।
-
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक भारत में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं को बढ़ाता/बढ़ाते है/हैं?
- दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता
- पश्चिमी विक्षोभ
- स्थलाकृति (ओरोग्राफिक प्रभाव)
- जलवायु परिवर्तन
सही विकल्प चुनें:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (d) 1, 2, 3 और 4
व्याख्या: ये सभी कारक भारत में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ नमी लाते हैं, स्थलाकृति ओरोग्राफिक वर्षा को बढ़ावा देती है, और जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता बढ़ाता है।
-
प्रश्न 5: भारत में आपदा प्रबंधन के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
(b) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए एक विशेष बल है।
(c) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) केवल भूस्खलन की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है।
(d) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में आपदा प्रबंधन ढांचे का आधार है।
उत्तर: (c) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) केवल भूस्खलन की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है।
व्याख्या: IMD मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने की प्राथमिक एजेंसी है, जिसमें वर्षा, चक्रवात, लू आदि शामिल हैं, न कि केवल भूस्खलन। भूस्खलन की भविष्यवाणी में कई अन्य एजेंसियां और कारक शामिल होते हैं।
-
प्रश्न 6: ‘संवहन धाराएँ’ (Convective Currents) और ‘तीव्र ऊपर उठती हवा’ (Updrafts) किस मौसमी घटना से सर्वाधिक संबंधित हैं?
(a) शीत लहरें
(b) पश्चिमी विक्षोभ
(c) बादल फटना
(d) मानसून का पीछे हटना
उत्तर: (c) बादल फटना
व्याख्या: संवहन धाराएँ और तीव्र ऊपर उठती हवाएँ बादलों में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने में मदद करती हैं, जो बादल फटने की घटना के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है।
-
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में बाढ़ से संबंधित आपदा प्रबंधन में एक चुनौती नहीं है?
(a) पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की सीमाएँ
(b) बुनियादी ढाँचे का लचीलापन
(c) प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय
(d) जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव
उत्तर: (c) प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय
व्याख्या: प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय एक चुनौती है, न कि समाधान। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन-सी चुनौती नहीं है, इसलिए प्रभावी समन्वय एक सकारात्मक विशेषता होगी, जबकि इसकी कमी एक चुनौती है।
-
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन-सा/से जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है/हैं?
1. वायुमंडल की अधिक नमी धारण करने की क्षमता में वृद्धि।
2. समुद्री धाराओं में कमी।
3. जेट स्ट्रीम में परिवर्तन।
सही विकल्प चुनें:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3
व्याख्या: बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वायुमंडल अधिक नमी धारण कर रहा है, जिससे तीव्र वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होती है। जेट स्ट्रीम में परिवर्तन भी मौसमी पैटर्न को प्रभावित करते हैं, जिससे चरम घटनाएँ बढ़ सकती हैं। समुद्री धाराओं में कमी का सीधा संबंध चरम मौसमी घटनाओं से कम है।
-
प्रश्न 9: भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों में शामिल हो सकता है/सकते हैं:
1. कृषि फसल का नुकसान।
2. जल-जनित बीमारियों का प्रसार।
3. बुनियादी ढाँचे का विनाश।
4. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा।
सही विकल्प चुनें:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3
व्याख्या: कृषि फसल का नुकसान, जल-जनित बीमारियों का प्रसार और बुनियादी ढाँचे का विनाश आपदाओं के सीधे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हैं। आपदाएँ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देतीं, बल्कि उसे बाधित करती हैं।
-
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन-सा ‘बिल्डिंग बैक बेटर’ (Building Back Better) के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(a) आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्निर्माण करना।
(b) आपदा के बाद पुनर्निर्माण के दौरान आपदा-लचीले और बेहतर बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
(c) केवल पारंपरिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके पुनर्निर्माण करना।
(d) आपदा के बाद आर्थिक गतिविधियों को तुरंत फिर से शुरू करना।
उत्तर: (b) आपदा के बाद पुनर्निर्माण के दौरान आपदा-लचीले और बेहतर बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
व्याख्या: ‘बिल्डिंग बैक बेटर’ का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि आपदा से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को केवल पुनर्निर्मित न किया जाए, बल्कि उन्हें पिछली स्थिति से भी अधिक लचीला, मजबूत और टिकाऊ बनाया जाए ताकि वे भविष्य की आपदाओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकें।
मुख्य परीक्षा (Mains)
-
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी रंग-कोडित अलर्ट प्रणाली का क्या महत्व है? पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए सटीक भविष्यवाणी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? चर्चा कीजिए।
-
“चरम मौसमी घटनाएँ अब ‘नया सामान्य’ बनती जा रही हैं।” भारत में हाल की भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इन घटनाओं के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए शमन और अनुकूलन रणनीतियों पर प्रकाश डालिए।
-
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भारत की आपदा प्रबंधन संरचना का विस्तार से वर्णन करें। भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक ‘आपदा-लचीले’ राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किन सुधारों की आवश्यकता है?